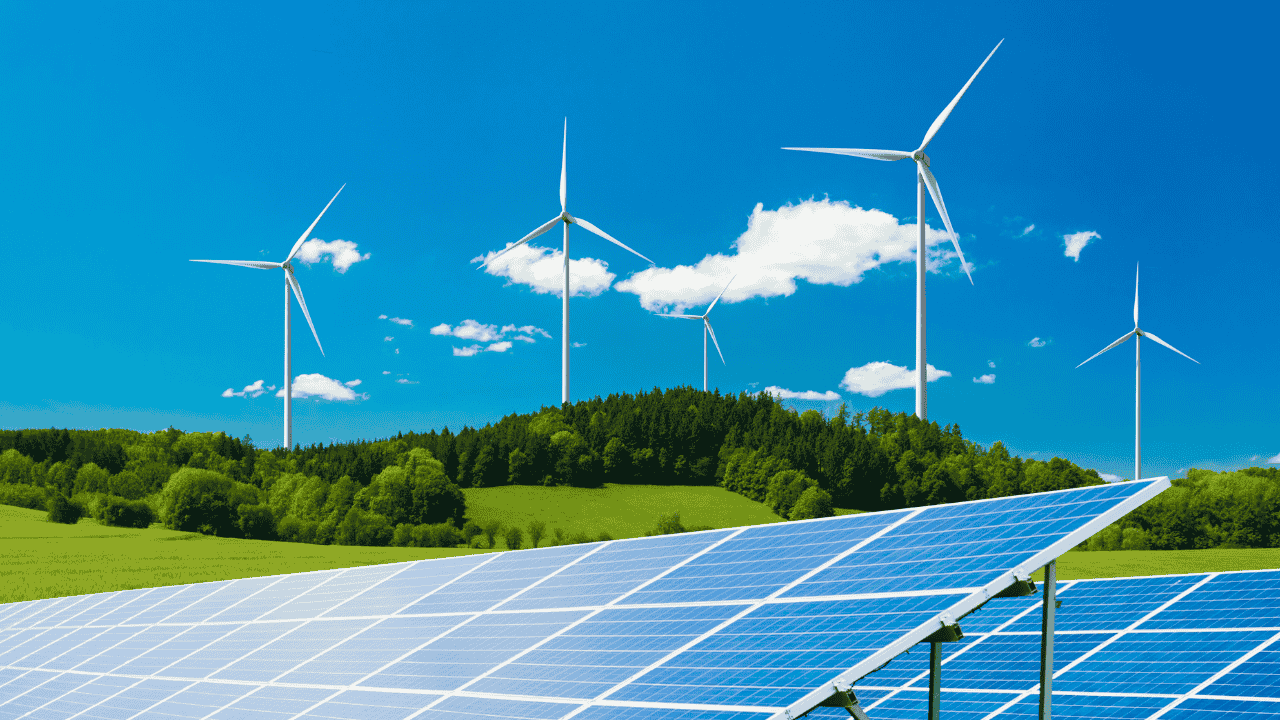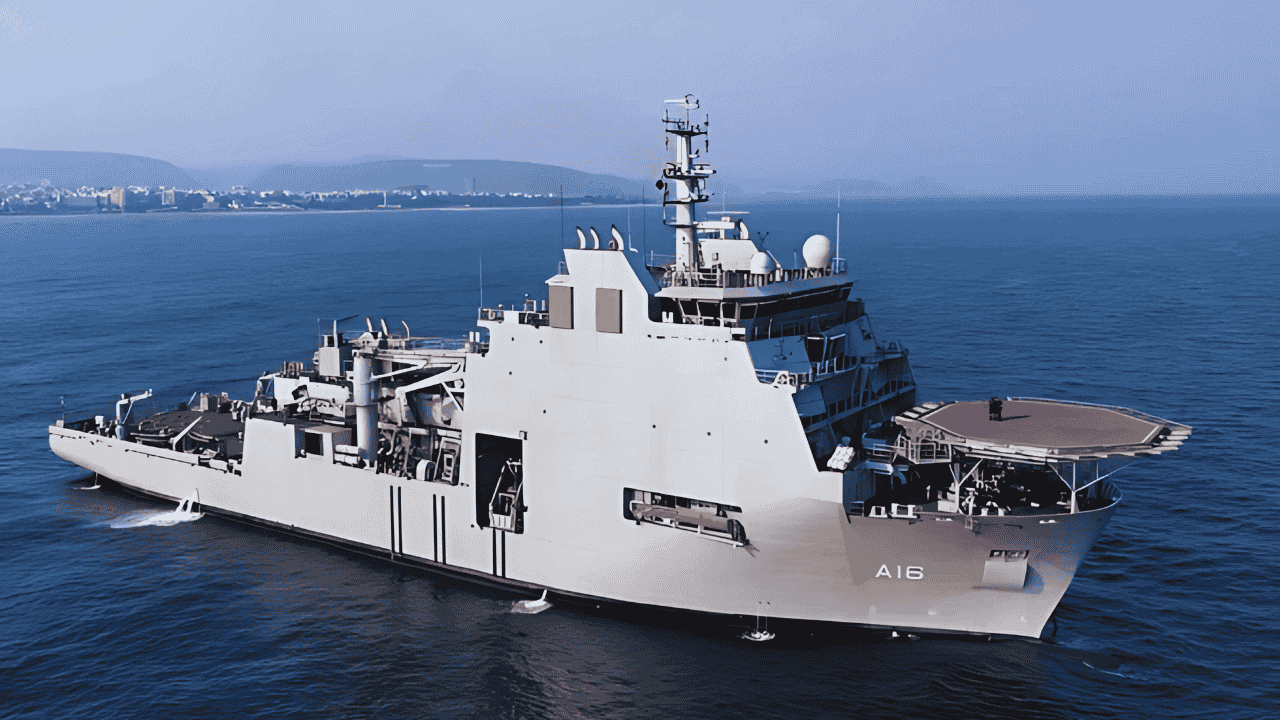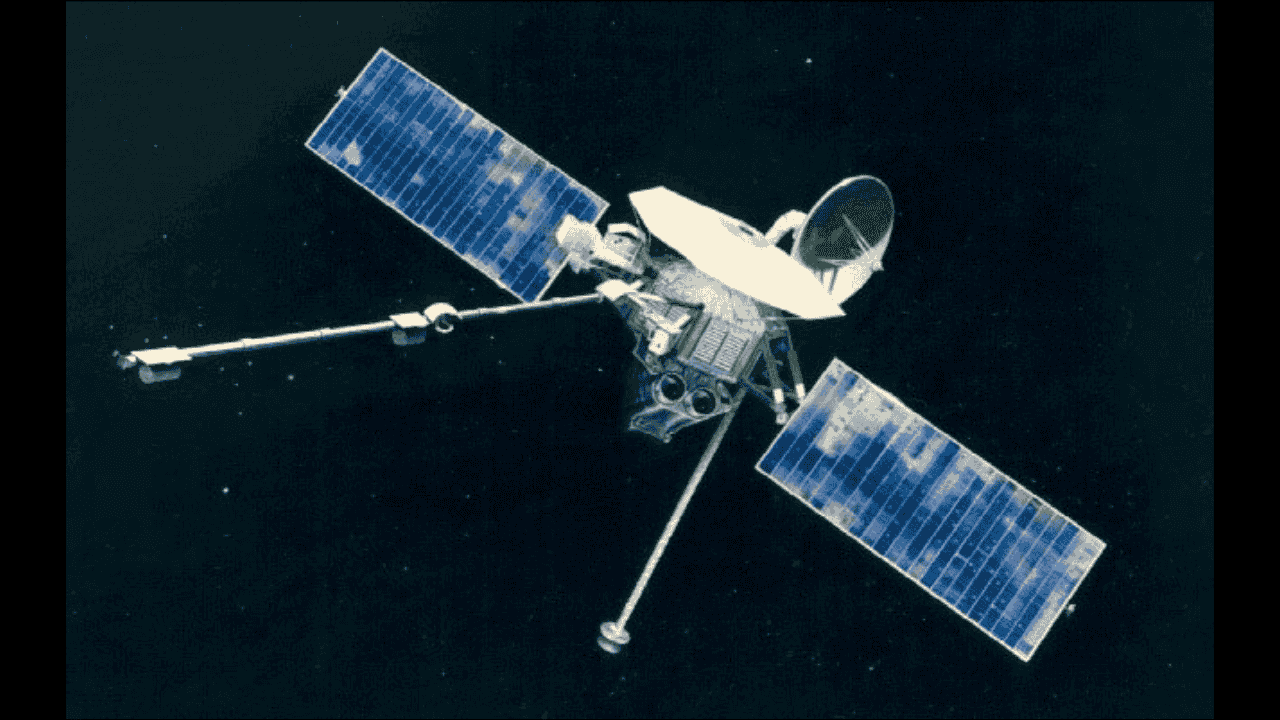परिचय
भारत अपनी तेज़ी से बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा क्षमताओं के साथ वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता जा रहा है। 2024 में देश ने रिकॉर्ड 24.5 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़कर दुनिया में तीसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि देश की आर्थिक और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। हालांकि, इस सफलता के पीछे एक गंभीर चुनौती छुपी हुई है - क्लाइमेट फाइनेंस की भारी कमी, जो भारत के 2030 के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है।
भारत की स्वच्छ ऊर्जा में रिकॉर्ड वृद्धि
2024 की उपलब्धियां
भारत ने 2024 में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावॉट तक पहुंच गई है, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 105.65 गीगावॉट और पवन ऊर्जा का 51.6 गीगावॉट है।
मुख्य आंकड़े:
2024 में 29.52 गीगावॉट की रिकॉर्ड वार्षिक क्षमता वृद्धि
सौर ऊर्जा में 23.83 गीगावॉट की वृद्धि, जो 2023 की तुलना में काफी अधिक है
पवन ऊर्जा में 3.4 गीगावॉट नई क्षमता का जोड़ना
रूफटॉप सौर में 53% की वृद्धि के साथ 4.59 गीगावॉट नई क्षमता
वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति
संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 2025 जलवायु रिपोर्ट में भारत को ब्राजील और चीन के साथ सौर और पवन ऊर्जा के विस्तार में अग्रणी विकासशील देश के रूप में मान्यता मिली है। भारत अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक है और चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्षमता रखने वाला देश है।
रोजगार और आर्थिक प्रभाव
बढ़ते रोजगार के अवसर
2023 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 1.02 मिलियन (10.2 लाख) लोगों को रोजगार मिला, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व और हरित रोजगार सृजन पर ध्यान दर्शाता है।
क्षेत्रवार रोजगार वितरण:
हाइड्रो पावर: 453,000 नौकरियां (सबसे बड़ा नियोक्ता)
सौर फोटोवोल्टिक: 318,600 लोगों को रोजगार
पवन ऊर्जा: 52,200 नौकरियां
बायो गैस: 85,000 नौकरियां
ऑफ-ग्रिड सौर: 80,000+ नौकरियां
जीडीपी में योगदान
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का भारत की जीडीपी वृद्धि में 5% योगदान है। यह क्षेत्र न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद कर रहा है, बल्कि आर्थिक विकास का भी महत्वपूर्ण साधन बन गया है।
क्लाइमेट फाइनेंस की चुनौती
निवेश की भारी आवश्यकता
भारत को अपने 2030 तक के 1.5°C जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए $1.5 ट्रिलियन से $2.5 ट्रिलियन के बीच निवेश की आवश्यकता होगी। यह राशि मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में चाहिए:
सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार
बिजली ग्रिड का आधुनिकीकरण और मजबूतीकरण
बैटरी स्टोरेज सिस्टम
ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक
टिकाऊ परिवहन प्रणाली
जलवायु-अनुकूल कृषि
वर्तमान वित्तीय स्थिति
हालांकि भारत में हरित वित्त बाजार बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी भी आवश्यकता से काफी कम है। दिसंबर 2024 तक, भारत ने $55.9 बिलियन का हरित, सामाजिक, और स्थिरता संबंधी ऋण जारी किया, जिसमें ग्रीन बॉन्ड का 83% हिस्सा है।
वित्तीय अंतर की समस्या:
वर्तमान में उपलब्ध निवेश आवश्यकता से काफी पीछे हैं
छोटे और मध्यम उद्यमों तक फंडिंग पहुंचाने में कठिनाई
ग्रामीण परियोजनाओं में निवेश की कमी
स्थानीय ऊर्जा योजनाओं का धीमा विकास
वित्तपोषण के नवाचार और समाधान
ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल
ब्लेंडेड फाइनेंस एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभर रहा है, जो सरकारी पूंजी, निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय अनुदान को मिलाकर जोखिम साझा करता है। यह मॉडल छोटे और मध्यम प्रोजेक्ट्स तक फंडिंग पहुंचाने में कारगर साबित हो रहा है।
ब्लेंडेड फाइनेंस के लाभ:
परियोजनाओं के जोखिम को कम करना
निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना
नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना
विकास लक्ष्यों के साथ वित्तीय रिटर्न का संतुलन
अन्य वित्तीय उपकरण
ग्रीन बॉन्ड: भारत में ग्रीन बॉन्ड बाजार तेजी से बढ़ रहा है और 2025 तक $45 बिलियन से अधिक का निवेश होने का अनुमान है।
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग: नई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना नए वित्तीय स्रोत प्रदान कर सकती है।
प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन: यह निवेशकों का भरोसा बढ़ाकर निवेश को आकर्षक बनाने में मदद कर रहा है।
सरकारी नीतियां और पहल
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक एक लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन आयात में कमी और 50 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी है।
पीएम सूर्य घर योजना
फरवरी 2024 में शुरू की गई यह योजना एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। दस महीनों के भीतर 7 लाख रूफटॉप सौर स्थापनाएं हो चुकी हैं।
निवेश प्रतिबद्धताओं
भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 32 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, 169 गीगावॉट क्षमता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना बोलियां निकली गई हैं।
भविष्य के अवसर और लक्ष्य
2030 के लक्ष्य
भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए प्रतिवर्ष औसतन 50 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़नी होगी।
दीर्घकालीन दृष्टि
2070 तक नेट-जीरो के लक्ष्य के लिए कुल $10.1 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। IRENA का अनुमान है कि यदि भारत 1.5°C-अनुकूल मार्ग अपनाए तो 2050 तक औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि 2.8% हो सकती है, जो G20 औसत से दोगुनी है।
तकनीकी नवाचार
भविष्य में भारत विकेंद्रीकृत ग्रिड, बैटरी-एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा, और हरित हाइड्रोजन जैसी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
चुनौतियों का समाधान
संस्थागत सुधार
घरेलू संस्थागत पूंजी को जुटाना (EPFO, LIC, पेंशन फंड)
नियामक सुधार और ESG ढांचे का विकास
हरित परियोजना पाइपलाइन का निर्माण
नीतिगत उपाय
कर छूट और राजकोषीय प्रोत्साहन से निजी निवेश को आकर्षित करना
क्रेडिट गारंटी और जोखिम साझाकरण तंत्र विकसित करना
ब्लॉकचेन और AI का उपयोग वित्त ट्रैकिंग और जोखिम मूल्यांकन के लिए
Why this matters for your exam preparation
UPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्व:
सामान्य अध्ययन III (पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा): यह टॉपिक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों, जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों, और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दों को कवर करता है। 24.5 GW सौर ऊर्जा जोड़ने और वैश्विक तीसरे स्थान पर पहुंचने जैसे तथ्य महत्वपूर्ण हैं।
सामान्य अध्ययन II (शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध): क्लाइमेट फाइनेंस की चुनौती ($1.5-2.5 ट्रिलियन की आवश्यकता) सरकारी नीति निर्माण, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, और भारत की वैश्विक जलवायु नेतृत्व की भूमिका को दर्शाती है।
सामान्य अध्ययन III (अर्थव्यवस्था): नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के जीडीपी में 5% योगदान, 10.2 लाख रोजगार सृजन, और ग्रीन बॉन्ड, ब्लेंडेड फाइनेंस जैसे वित्तीय नवाचार आर्थिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य:
भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता: 220.10 GW
2024 में सौर ऊर्जा जोड़ना: 24.5 GW
वैश्विक रैंकिंग: तीसरा स्थान (सौर ऊर्जी में)
2030 का लक्ष्य: 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता
रोजगार: 1.02 मिलियन लोग (2023)
मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न:
"भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन की सफलताओं के बावजूद क्लाइमेट फाइनेंस एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस वित्तीय अंतर को पाटने के लिए नवाचारी वित्तीय तंत्रों की आवश्यकता और भूमिका का विश्लेषण करें।"