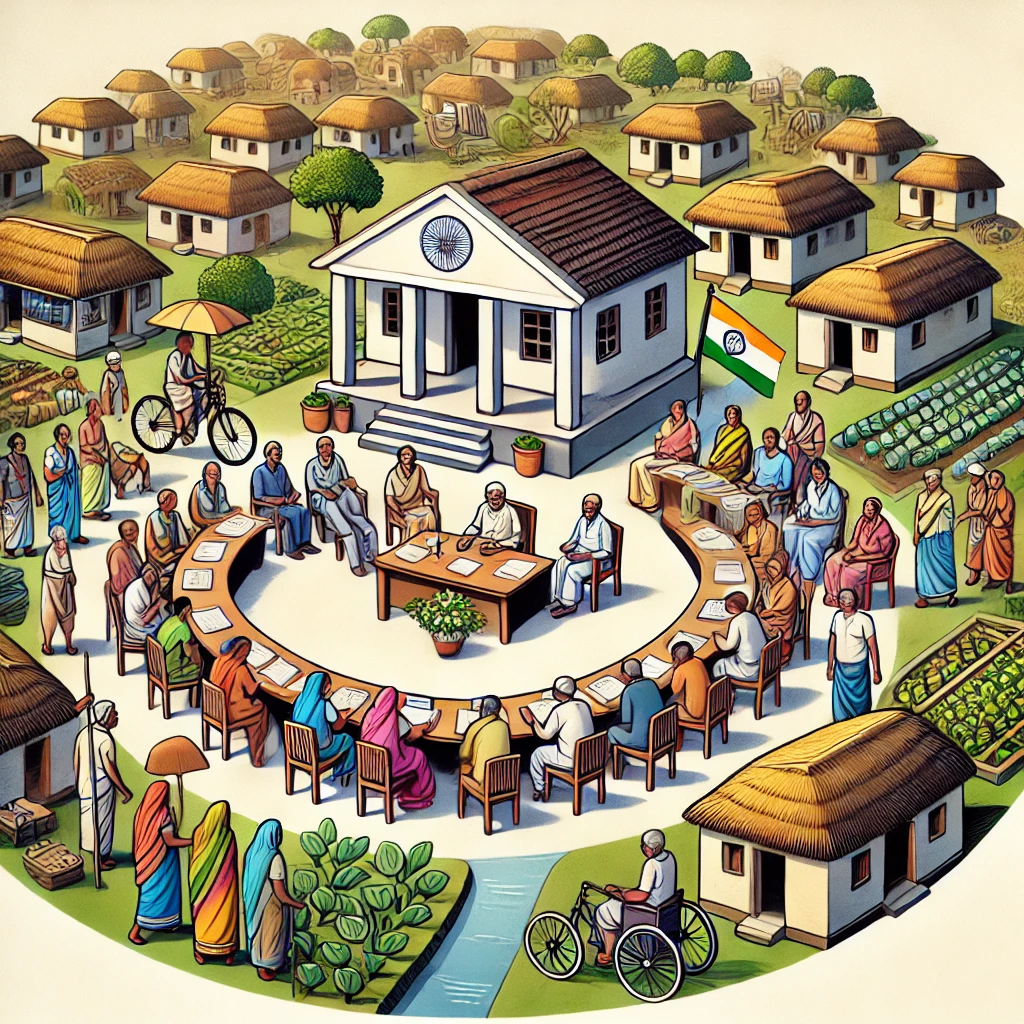प्रस्तावना
चीन द्वारा यारलुंग त्सांगपो नदी (भारत में ब्रह्मपुत्र) पर दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध बनाने की योजना से पर्यावरण, कृषि उत्पादकता और भू-राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह बांध तिब्बत के ग्रेट बेंड के पास प्रस्तावित है, जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसका असर भारत और बांग्लादेश के लाखों लोगों पर पड़ेगा।
ब्रह्मपुत्र नदी का सामरिक महत्व
ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नाम
ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत के केमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, यारलुंग त्सांगपो के रूप में पूर्व की ओर बहती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इसे सियांग/दिहांग नदी कहा जाता है। असम में यह ब्रह्मपुत्र बन जाती है और बांग्लादेश में जमुना नदी के रूप में बहती है, अंततः पद्मा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है।
अद्वितीय प्रवाह विशेषताएँ
ब्रह्मपुत्र नदी की ढलान तिब्बत में बहुत अधिक होती है, जो जलविद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल है। लेकिन भारत में प्रवेश करने के बाद इसे डिबांग, लोहित और सुबनसिरी जैसी भारी बारिश से पोषित सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिससे जल स्तर और गाद की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है और माजुली (दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप) जैसे नदीय द्वीपों का निर्माण होता है।
चीन के ब्रह्मपुत्र बांध से जुड़े खतरे
पर्यावरणीय प्रभाव
प्राकृतिक प्रवाह में बाधा – बांध से जल वितरण में परिवर्तन होगा, जिससे कृषि और जैव विविधता प्रभावित होगी।
बाढ़ और सूखे का खतरा – चीन द्वारा नदी के प्रवाह पर नियंत्रण से मानसून में बाढ़ और शुष्क मौसम में सूखा बढ़ सकता है।
भूकंपीय संवेदनशीलता – यह क्षेत्र एक उच्च भूकंप-संभावित जोन में स्थित है, जिससे बांध का भूकंप से क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है।
जैव विविधता पर खतरा – यह परियोजना पूर्वी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, जो विलुप्तप्राय प्रजातियों का घर है।
भारत की जलविद्युत परियोजनाओं पर प्रभाव
भारत में ब्रह्मपुत्र पर कई जलविद्युत परियोजनाएँ हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
लोअर सुबनसिरी (2,000 मेगावाट)
डिबांग (3,000 मेगावाट)
कामेंग (600 मेगावाट)
तीस्ता-V (510 मेगावाट)
अगर चीन द्वारा नदी के प्रवाह को नियंत्रित किया गया, तो इन परियोजनाओं को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है।
भू-राजनीतिक प्रभाव
चीन की जलविद्युत विस्तार नीति
चीन, जो पहले ही दुनिया में सबसे अधिक बांधों का मालिक है, अब सीमा-पार नदियों को अपने हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयोग कर रहा है। इसका सीधा असर भारत और बांग्लादेश जैसे निचले प्रवाह वाले देशों पर पड़ेगा, जो ब्रह्मपुत्र पर जल सुरक्षा और कृषि के लिए निर्भर हैं।
भारत की प्रतिक्रिया और सीमा-पार सहयोग की आवश्यकता
हालांकि भारत और चीन के बीच कुछ समझौते और 2006 में स्थापित विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र मौजूद हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक जल-साझाकरण संधि नहीं है।
संभावित समाधान:
वास्तविक समय हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझाकरण – पारदर्शी जल-साझाकरण समझौते की स्थापना।
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव – युनेस्को, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जल संगठन जैसे वैश्विक संस्थानों को शामिल करना।
भारत की जलविद्युत अवसंरचना को मजबूत करना – घरेलू बांध परियोजनाओं का विस्तार करना, जिससे चीन के जल प्रवाह नियंत्रण पर निर्भरता कम हो।
सतत नदी घाटी प्रबंधन – बांग्लादेश और भूटान के साथ संयुक्त संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष
चीन का प्रस्तावित ब्रह्मपुत्र बांध गंभीर पर्यावरणीय, कृषि और भू-राजनीतिक खतरे उत्पन्न कर सकता है। रणनीतिक कूटनीतिक वार्ता, वास्तविक समय हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझाकरण, और भारत की जल प्रबंधन नीतियों को मजबूत करना आवश्यक है ताकि जल सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन बना रहे।
चीन के ब्रह्मपुत्र बांध की योजना भारत और बांग्लादेश के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। जानिए इस परियोजना के पर्यावरणीय, कृषि और भू-राजनीतिक प्रभावों के बारे में।
ब्रह्मपुत्र बांध, चीन की जलविद्युत परियोजनाएँ, यारलुंग त्सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी, भू-राजनीतिक चिंताएँ, पर्यावरणीय प्रभाव, भारत-चीन जल विवाद, सीमा-पार नदियाँ, भारतीय जलविद्युत परियोजनाएँ, जलवायु परिवर्तन, हिमालयी पारिस्थितिकी
External Linking
विश्व बैंक पर जल साझाकरण संधियाँ
युनेस्को रिपोर्ट: सीमा-पार जल सहयोग
By Team Atharva Examwise #atharvaexamwise